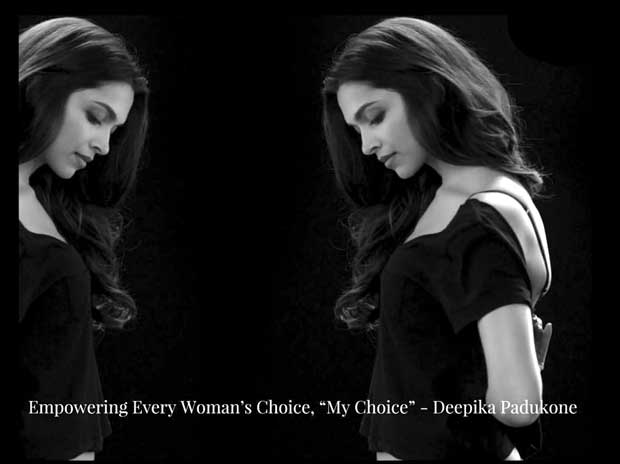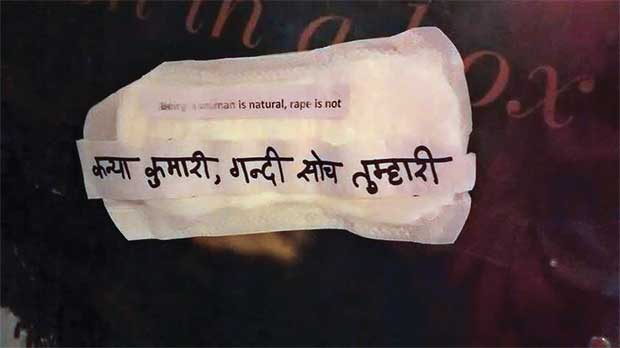इलस्ट्रेशनः आनंद नॉरम
आज ही राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत से सीधे सऊद परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने सऊदी अरब निकले हैं. अमेरिका का सऊद-परिवार से बड़ा खास रिश्ता है. उसी ठग सऊद परिवार से जो अरब-अफ्रीका-दक्षिण एशिया में पेट्रो-डॉलर के जरिये अपनी तमाम नाजायज औलादों से इस पूरे भूभाग को जहन्नुम बनाए हुए है. सिर्फ इसलिए की कहीं उसके मालिकों का शस्त्र-उद्योग मंदी का शिकार न हो जाए और यहां की अवाम पूंजीवाद के उन मोहरों को अपदस्थ न कर दे जो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक हुक्मरान बने बैठे हैं. लेकिन ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ वाले इस दौर में भी कोई माई का लाल अमेरिका और यूरोप से यह सवाल नहीं पूछता कि मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्रांति, नास्तिकता, नारीवाद जैसे महान सिद्धांत सऊदी अरब के मामले में निलंबित अवस्था में ही पड़े रहेंगे क्या? और हर तरह की आजादियों के चैंपियन अमेरिका का सबसे ‘घनिष्टतम सहयोगी’ सऊदी अरब आखिर कब तक गैर जवाबदेही काल में मौज करेगा? सऊदी अरब की खड़ी की गई अवैध फौजों की हरकतों पर जवाबदेही क्या उन निरीह सेक्युलर सहिष्णु मुसलमानों की ही बनती है जो शर्ली हेब्दो हत्याकांड की सबसे पहले निंदा करते हैं. लेकिन साथ ही उन्हें ये भी जरूरी लगता है की अश्लील कार्टूनों के जरिये उनके पैगंबर का उपहास न उड़ाया जाए.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या ‘फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन’ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुल जमा सत्तर-पिछत्तर साल पहले, दुनिया के समक्ष लाया गया सिद्धांत है. ये प्रबोधन काल में पैदा हुई वैयक्तिक स्वतंत्रताओं के सबसे परिष्कृत सिद्धांतों में से एक है. यानी यूरोप में मध्यकाल से शुरू हुए पुनर्जागरण से लेकर लोकतांत्रिक व औद्योगिक क्रांतियों के दौर में हुए सघन सामाजिक आत्ममंथन, वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रगतिशीलता के सिद्धांतों के चरम बिंदु पर पहुंचकर हासिल, वो उसूल जिसको पाने में यूरोप की छह से ज़्यादा सदियां खर्च हुईं और जिसका सत है ‘यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स-1948′.
इसमें यह भी याद रखना होगा की यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कोई ऐसा पश्चिमी राष्ट्र नहीं है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्पूर्ण रूप से दी गयी हो. खुद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स-1948′ भी किंतु-परंतु से मुक्त न हो कर इनसे लदा-फंदा है. यानी कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी नामंज़ूर हैं. इसी के साथ पश्चिम के सभी राष्ट्र-राज्यों के अपने-अपने संविधानों में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीम या परम सिद्धांत न होकर कई किंतु-परंतु में लिपटा हुआ है. खुद भारत का संविधान, जिसे एक प्रोग्रेसिव, दूरअंदेश और आधुनिकता का वाहक-दस्तावेज माना जाता है, उसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीम परम-सिद्धांत न हो कर कुछ जरूरी सावधानियों से लैस है.
ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, कार्टून जैसी व्यंग्यात्मक और उपहास के लिए इस्तेमाल होनेवाली अभिव्यक्ति की शैली को उस समाज के मूल्यों से भिड़ा देना, जिस समाज ने अभी आत्म-मंथन के मुहाने पर सिर्फ पहला कदम रखा है, न सिर्फ शरारतपूर्ण है, बल्कि उस समाज के प्रगतिशीलों और आधुनिकों को असमंजस और ग्लानि से भरना है. इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में एशिया और अफ्रीका के देशों द्वारा ‘यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स-1948′ पर सरकारों की मोहर लगना एक बात है और इनके अवाम के मन-मस्तिष्क में इन सिद्धांतों को उतरना बिल्कुल दूसरी बात है या कहें कि टेढ़ी खीर है.
इस कड़ी में याद रखना होगा की यही पश्चिम राष्ट्रों का वह गिरोह है जिसने 70 और 80 के दशक में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, इंडोनेशिया सहित तमाम एशियाई देशों में उदार, आधुनिक और सेक्युलर शासकों का तख्ता पलट करवाकर अपने पिट्ठू गद्दीनशीन करवाए थे. इन पिट्ठुओं ने अवाम के बीच वैधता पाने के लिए अल्लाहमियां का एजेंट बन धार्मिक कट्टरवादी अनुकूलन का सहारा लिया. मोसद्दिक, भुट्टो, नजीबुल्लाह जैसे अवामी सेक्युलर शासकों को मौत के घाट उतारकर अमेरिकी पिट्ठुओं को धार्मिक कट्टरता के सहारे लाचार अवाम पर थोपने का अपराधी पश्चिम, अब जेहादियों, तालिबानों, ‘इस्लामिक-स्टेट’ से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने का ढोंग कर रहा है.
ऐसे सियासी चक्रव्यूह में घिरे और पश्चिम की नफरत के शिकार समाजों में इस्राइल-अमरीका-यूरोप द्वारा पैगंबर साहब का वस्त्रहीन अश्लील, बेइज्जत करता हुआ कार्टून बनाकर अगर कोई प्रगतिशीलता लाने का सपना देख रहा है तो उसने इसके नतीजों पर भी गौर किया होगा. दशकों से पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण के शिकार और भ्रष्ट राजतन्त्र से आजिज नौजवान जब फिदायीन बन खुद को उड़ा सकते हैं तो पेशावर-पेरिस में दूसरों को मारकर, मर भी सकते हैं. जो खुद मरने ही आया है उसे आप कौन-सी सजा दे देंगे?
भारत का संविधान, जिसे एक प्रोग्रेसिव और आधुनिकता का वाहक-दस्तावेज माना जाता है, उसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कुछ जरूरी सावधानियों से लैस है
लेकिन मसला तो ये है की एशिया-अफ्रीका के समाजों में धर्म की सियासत को सहिष्णु, सुधारवादी और सहनशील बनाने में लगे उदारवादी, आधुनिक लोग कैसे अपनी मुहिम जारी रखें? जो शार्ली हेब्दो अपने पन्नों पर यहूद-मुखालिफत और इस पर कार्टून की इजाजत नहीं देता उसी शार्ली हेब्दो के मुहम्मद साहब पर बनाए अश्लील कार्टून का लिबरल-मॉडरेट मुसलमान समर्थन करें? ये कैसा इम्तेहान है? आखिर ये धर्म के मूल में आस्था रखनेवाले लोग हैं. इनको अल्लाह और उसके पैगम्बर पर भरोसा है. ये उस मुल्ला वर्ग के विरोधी हैं जिन्होंने धर्म की डरावनी और जड़ व्याख्याएं करके समाज को अपना गुलाम बनाया और तालिबान, बोको हरम, इस्लामिक-स्टेट जैसे संगठनो को विश्वसनीयता प्रदान की. मेरा दावा है की पेशावर-पेरिस काण्ड करनेवाले अपराधी किसी न किसी सिद्धांतकारी उलेमा-गिरोह के प्रभाव में हैं, लेकिन मीडिया, पश्चिम जगत और सिविल सोसाइटी उधर से आंख मूंद लेता है.
खैर, 1990 के बाद से जब दुनिया भर में साम्यवादी व्यवस्थाएं खत्म हुईं, तभी से ऐसे भस्मासुर पैदा किए गए जिनको दिखाकर हथियार उद्योग को सरसब्ज रखा जा सके. तेल के कुओं पर अवैध कब्जा, हथियार मंडी पर कब्जा, और दुनियाभर के बाजारों पर कब्जा जिन्हें हर हाल में चाहिए उन्हें कट्टरवाद और धार्मिक श्रेष्ठतावाद की खेती करनी ही है.
लेकिन हमें शिकायत उस सिविल सोसाइटी, मीडिया और प्रगतिशीलता से है जो आजादी विरोधी फतवों पर तो फिक्रमंद होती है, लेकिन जब शिक्षित-प्रशिक्षित आम मुसलमानों को किराए पर मकान नहीं मिलता तो आंखें मूंद लेती है. जो शर्ली हेब्दो के कार्टून का समर्थन करती है पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के कार्टून में आहत भावनाओं की कद्र करती है, जो प्रोफेसर आशीष नंदी से दलितों के प्रति नस्लवादी बयान के लिए माफी मंगवाती है पर प्रवीण तोगड़िया के मुसलमानों को बेइज्जत करनेवाले सैकड़ों बयानों पर दूसरी तरफ देखने लगती है, जो असम के नरसंहारों को तो सामान्य अपराध मानती है पर पेशावर के नरसंहार को इस्लामी कृत्य मानती है, जो उपराष्ट्रपति डॉ हामिद अंसारी के प्रोटोकॉल के पालन को देशद्रोह कहनेवालों से सवाल तक नहीं करती.
सियासी सहीपने के आग्रहों से आजिज आ कर एक मुसलमान ने ‘Muslim iCondemn app’ बना लिया है, जिसे रोज मोबाइल फोन में क्लिक करके दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान द्वारा किए गए अपराध की निंदा कर हम भी जवाबदेही से मुक्त हो जाएंगे. बाकी तो जैसा अमेरिका बहादुर तय करे.

 June 17, 2015
June 17, 2015